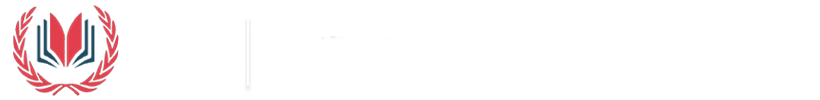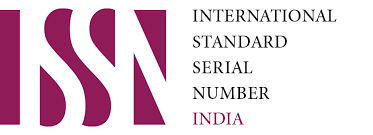आत्मनिर्भरता: भारतीय ज्ञान परंपरा
DOI:
https://doi.org/10.8224/journaloi.v74i1.615Abstract
आत्मनिर्भरता एक ऐसी स्थिति या गुण है जिसमें व्यक्ति, समाज, या राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम होता है। इसका मतलब है कि बाहरी सहायता, संसाधनों, या निर्भरता के बिना आत्मनिर्भर बनकर समस्याओं का समाधान करना और आवश्यकताओं को पूरा करना। यह मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
भारत की प्राचीन, समृद्ध और बहुस्तरीय बौद्धिक परंपरा को संदर्भित करती है। यह परंपरा वैदिक, शास्त्रीय और लोक ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान, कला, दर्शन, और साहित्य तक फैली हुई है। इसमें ज्ञान को केवल सांसारिक समझ के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सत्य की खोज के रूप में देखा गया है।
वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिन्हें 'अपौरुषेय' और 'अनादि' माना जाता है। उपनिषद ज्ञान के गूढ़ और दार्शनिक पक्षों पर केंद्रित हैं, जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गहरे विचार प्रस्तुत करते हैं। भारतीय दर्शन छह प्रमुख आस्तिक दर्शनों (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत) और चार नास्तिक दर्शनों (बौद्ध, जैन, चार्वाक, आजीविक) में विभाजित है। इन विचारधाराओं ने तर्क, चेतना, ब्रह्मांड, नैतिकता और मुक्ति पर गहन चर्चा की है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने अंकगणित, त्रिकोणमिति और खगोलशास्त्र में अग्रणी योगदान दिया। आयुर्वेद (चरक संहिता, सुश्रुत संहिता) प्राचीन चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख स्रोत है।